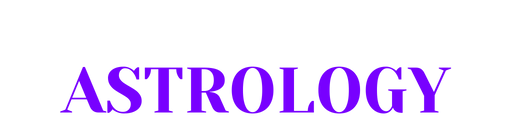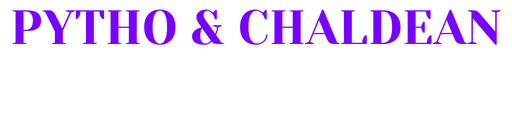छान्दोग्य उपनिषद – Chandogya Upanishads
Chandogya Upanishad Hindi : सामवेद की तलवकार शाखा में इस उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। छान्दोग्य उपनिषद (Chandogya Upanishad Pdf) मे दस अध्याय हैं। इसके अन्तिम आठ अध्याय ही इस उपनिषद में लिये गये हैं। नाम के अनुसार इस उपनिषद का आधार ‘छन्द’ है, इसका यहाँ व्यापक अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है। इसे यहाँ ‘आच्छादित करने वाला’ माना गया है। साहित्यिक कवि की भांति ऋषि भी मूल सत्य को विविध माध्यमों से अभिव्यक्त करता है। वह प्रकृति के मध्य उस परमसत्ता के दर्शन करता है। इसमें ॐकार (‘ॐ’) को सर्वोत्तम रस माना गया है।
प्रथम अध्याय
प्रथम अध्याय में तेरह खण्ड हैं। इनमें ‘साम’ के सार रूप ‘ॐकार’ की व्याख्या की गयी है तथा ‘ॐकार’ की अध्यात्मिक, आधिदैविक उपासनाओं को समझाते हुए विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट किया है।
पहला खण्ड
ॐकार सर्वोत्तम रस है। सर्वप्रथम उद्गाता ‘ॐ’ का उच्चारण करके सामगान करता है। वह बताता है कि समस्त प्राणियों और पदार्थों का रस अथवा सार पृथिवी है। पृथ्वी का सार जल है, जल का रस औषधियां हैं, औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाणी है, वाणी का रस साम है और साम का रस उद्गीथ ‘ॐकार’ है।
यह ओंकार सभी रसों में सर्वोत्तम रस है। यह परमात्मा का प्रतीक होने के कारण ‘उपास्य’ है। जिस प्रकार स्त्री-पुरुष के मिलन से एक-दूसरे की कामनाओं की पूर्ति होती है, उसी प्रकार इस वाणी, प्राण और ऋचा तथा साम (गायन) के संयोग से ‘ॐकार’ का सृजन होता है।’ॐकार’ अनुभूति-जन्य है, जिसे अक्षरों के गायन से अनुभव किया जाता है। यह अक्षरब्रह्म की ही व्याख्या है।
दूसरा खण्ड :
देवासुर संग्राम के समय देव परस्पर विचार करके उद्गीथ ‘ॐकार’ की उपासना करते हैं और असुरों के पराभव की प्रार्थना करते हैं। आसुरी शक्ति से बचने के लिए ॐकार साधना का विधान बताया गया है। देवों की वाणी, उनके देखने व सुनने की शक्ति, मन की एकाग्रता, प्राण-शक्ति और अन्य ऋषियों की उपासना को असुर नष्ट कर डालते हैं। वे बार-बार ॐकार की उपासना में विघ्न डालते रहते हैं।
तीसरा खण्ड :
इस खण्ड में आधिदैविक रूप से ॐकार की उपासना की जाती है; क्योंकि मधुर उद्गान प्राणी में प्राणों को संचार करता है। इस प्रकार वह अन्धकार और सभी प्रकार के भय से प्राणी को मुक्त करने की चेष्टा करता है। प्राण और सूर्य को वह समान मानता है। अत: इस प्राण और उस सूर्य में ही ॐकार को मानकर उपासना करनी चाहिए।
उद्गाता जिस ‘साम’ के द्वारा उद्गीथ की उपासना करे, सदा उसी का चिन्तन भी करे। जिस छन्द के द्वारा स्तुति करता हो, उस छन्द का चिन्तन करे। जिन स्तोत्रों से स्तुति करता हो, उस स्तोत्रों का चिन्तन करे। जिस दिशा का चिन्तन करता हो, उस दिशा का चिन्तन करे। इस प्रकार अन्त में अपने आत्म-स्वरूप और कामना आदि का चिन्तन प्रमाद-रहित होकर करे। तभी उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।
चौथा खण्ड :
इस खण्ड में ‘ॐ’ को ही उद्गीथ माना है और उसी की उपासना करने की बात कही है। यद्यपि ‘ॐ’ एक स्वर है, तथापि यह अक्षर, अमृत और अभय-रूप ब्रह्म का प्रतीक है। समस्त देवगण और उपासक इस एक अक्षर-ब्रह्म ‘ॐकार’ में प्रविष्ट होकर अमरत्व और अभय को प्राप्त करते हैं।
पांचवां खण्ड :
इस खण्ड में ‘उद्गीथ’ और ‘प्रणव’ ॐ को एक रूप ही माना गया है। सूर्य ही उद्गीथ है, प्रणव है। यह सतत गतिशील रहकर ‘ॐ’ का उच्चारण करता रहता है। आगे कहा गया है कि मुख्य प्राण के रूप में ही उद्गीथ की उपासना करनी चाहिए।
छठा खण्ड :
इस खण्ड में पृथ्वी को ‘ऋक् और अग्नि को ‘साम’ कहा गया है। यह अग्नि-रूप साम, पृथ्वी-रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है। अत: ऋचा में इसी अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है। पृथ्वी को ‘सा’ और अग्नि को ‘अम’ मानकर दोनों के मिलन से ‘साम’ बनता है। ऋषि आगे कहते हैं कि अन्तरिक्ष ही ‘ऋक्’ है और वायु ‘साम’ है। वह वायु-रूप साम अन्तरिक्ष-रूप ऋक् में प्रतिष्ठित है। अत: ऋचा में अधिष्ठित साम का गायन किया जाता है।
इसी प्रकार नक्षत्र, आकाश व आदित्य को ‘ऋक्’ मानकर और क्रमश: चन्द्र, आदित्य और नीलवर्ण मिश्रित कृष्ण प्रकाश को ‘साम’ मानकर उनकी उपासना की गयी है। ऋग्वेद और सामवेद उसी परमपुरुष की उपासना गायन द्वारा करते हैं। वह परमपुरुष आदित्य आदि से भी ऊंचे लोकों तथा देवों का नियामक है और देवों की कामनाओं का पूरक है। यह उद्गीथ की आधिदैविक उपासना का स्वरूप है।
सातवां खण्ड :
अध्यात्मिक उपासना क्या है?
इस खण्ड में अध्यात्मिक उपासना का वर्णन है। वाणी-रूप ऋक् में प्राण-रूप साम, चक्षु-रूप ऋक् में आत्मा-रूप साम, श्रोत-रूप ऋक् में मन-रूप साम, नेत्रों की श्वेत आभा-रूप ऋक् में नील आभायुक्त स्याम-रूप साम, नेत्रों के मध्य स्थित पुरुष ही ऋक् और साम है। यही ब्रह्म है, यही आदित्य के मध्य स्थित पुरुष है, यही मनुष्य की समस्त कामनाओं को अपने अधीन रखता हैं जो इस रहस्य को जानकर गायन करते हैं, वे इसी पुरुष (ब्रह्म) का गायन करते हैं। इसी के द्वारा उद्गाता सभी लोंकों के समस्त भोगों की प्राप्त करता है।
आठवां खण्ड :
इस खण्ड में बताया है कि तीन ऋषि उद्गीथ सम्बन्धी विद्या में पारंगत थे। शालवान पुत्र शिलक, चिकितायन के पुत्र दालभ्य और जीवल के पुत्र प्रवाहण। एक बार परस्पर चर्चा करते हुए शिलक ने पूछा—’साम की गति (आश्रय) क्या है?’
दालभ्य ने उत्तर दिया-‘स्वर।’
शिलक- स्वर की गति क्या है?’
दालभ्य-‘प्राण।’
शिलक-‘प्राण की गति क्या है?’
दालभ्य-‘अन्न।’
शिलक-‘अन्न की गति क्या है?’
दालभ्य-‘जल।’
इसी प्रकार प्रश्न पूछने पर जल की गति ‘स्वर्ग, ‘ स्वर्ग की गति पूछने पर दालभ्य ने कहा कि स्वर्ग से बाहर साम को किसी अन्य आश्रम में नहीं रखा जा सकतां साम की स्वर्ग-रूप में ही स्तुति की गयी है, परन्तु शिलक इससे सन्तुष्ट नहीं हुआ। तब दालभ्य के पूछने पर शिलक ने कहा-‘यह लोक।’ परन्तु शिलक के उत्तर से प्रवाहण सन्तुष्ट नहीं हुआ। तब इस लोक की गति के बारे में प्रवाहण से प्रश्न पूछा गया।
नौवां खण्ड :
इस खण्ड में प्रवाहण शिलक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है-‘इस लोक का आश्रय अथवा गति आकाश है; क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी और पदार्थ अथवा तत्त्व इसी आकाश से उत्पन्न होते हैं और इसी में लीन हो जाते हैं। अत: आकाश ही इस लोक का आश्रय है। वही श्रेष्ठतम उद्गीथ है और वही अनन्त रूप है। जो विद्वान इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता है, उसे परम उत्कृष्ट जीवन प्राप्त होता है और परलोक में भी श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त होता है।’
दसवां खण्ड :
एक समय की बात है, ओलों की वृष्टि से कुरुदेश की खेती नष्ट हो गयी। उस समय इम्य ग्राम में चक्र ऋषि के पुत्र उषस्ति अपनी कम उम्र पत्नी के साथ बड़ी दीन अवस्था में रहने लगे थे। एक दिन उषस्ति ने अत्यन्त घुने उड़द खाने वाले एक निर्धन महावत से भिक्षा मांगी। तब उसने कहा-‘ऋषिवर! इन जूठे उड़द के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है।’
उषस्ति ने कहा-‘इन्हीं में से मुझे दे दो।’ महावत ने उड़द दे दिये और जल पीने को दिया। उस पर उषस्ति ने कहा कि जल पीने से उन्हें जूठा जल पीने का दोष लग जायेगा।
महावत ने कहा-‘क्या ये उड़द जूठे नहीं है?’
उषस्ति-‘इन्हें खाये बिना मैं जीवित नहीं रह सकता था, परन्तु जल तो मुझे कहीं भी मिल जायेगा।’उषस्ति ऋषि ने उन उड़द का एक भाग खाकर, दूसरा भाग अपनी पत्नी को ले जाकर दिया, परन्तु वह पहले ही बहुत-सी भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी। अत: उसने उड़द लेकर रख लिये। दूसरे दिन प्राप्त:काल उषस्ति ऋषि ने अपनी पत्नी से थोड़ा-सा अन्न मांगा। उषस्ति ऋषि की पत्नी ने उनके दिये उड़द उन्हें सौंप दिये।
ऋषि उषस्ति उन्हें खाकर समीप के राजा के यहाँ होने वाले यज्ञ में गये। वहां जाकर उन्होंने प्रस्तोता से कहा-‘जिस देवता की आप स्तुति करते हो, यदि उसे जाने बिना स्तुति करोगे, तो आपका सिर गिर जायेगा।’ यही बात उन्होंने उद्गाता के पास जाकर कही और प्रतिहर्ता से भी कही। उनकी बात सुनकर प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता अपने-अपने कर्मों से विरत होकर बैठ गये।
ग्यारहवां खण्ड :
यह देखकर यजमान राजा ने कहा-‘मैं आपको जानना चाहता हूँ ऋषिवर!’
उषस्ति ने अपना परिचय दिया-‘मैं चक्र का पुत्र उषस्ति हूँ।’
तब राजा ने कहा-‘आप ही हमारे यज्ञ को पूर्ण करायें।’
उषस्ति ने तब कहा-‘ऐसा ही हो। अब मैं इन्हीं प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता से यज्ञ कराऊंगा। आप जितना धन इन्हें देंगे, उतना ही धन मुझे भी देना।’राजा की स्वीकृति के बाद जब उषस्ति यज्ञ कराने के लिए तैयार हुए, तो प्रस्तोता ने देवता के बारे में पूछा। तब उषस्ति ने कहा-‘वह देवता प्राण है। प्रलयकाल में सभी प्राणी प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और उत्पत्ति के समय ये प्राण से ही उत्पन्न हो जाते हैं। यह ‘प्राण’ ही स्तुत्य देव है। यदि आप उसे जाने बिना स्तुति करते, तो मेरे वचन के अनुसार आपका मस्तक निश्चय ही गिर जाता।’
इसी प्रकार उद्गाता के पूछने पर उन्होंने ‘आदित्य’ को देवता बताया और उदीयमान सूर्य की उपासना करने की बात कही। प्रतिहर्ता के पूछने पर उन्होंने ‘अन्न’ को देवता बताया; क्योंकि अन्न के बिना प्राणी का जीवित रहना असम्भव है।
बारहवां खण्ड :
इस खण्ड में शौव (शौवन) उद्गीथ का वर्णन है। शौवन का अर्थ श्वान (कुत्ता) से है, परन्तु यहाँ श्वान का अर्थ कुत्ते से नहीं, गतिशीलता से है। यह गतिशीलता ही ‘प्राण’ है। इस प्रसंग में ऋषिपुत्र स्वाध्याय प्रकृति के मध्य श्वेत (निर्मल) श्वान (प्राण-प्रवाह) से साक्षात्कार करते हैं शुद्ध श्वान (प्राण) को उद्गीथ मानकर की गयी साधना फलित होती है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार बकदालभ्य अथवा ग्लाब मैत्रेय स्वाध्याय के लिए जलाशय के निकट गये। वहां निर्मल श्वान का प्रकटीकरण हुआ।
उससे कुछ अन्य विकारग्रस्त श्वान कहने लगे कि वे भूखे हैं। उनके लिए वे ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने सभी को प्रात:काल आने के लिए कहकर भेज दिया। दूसरे दिन प्रात:काल उनके आने पर सभी मिलकर प्रार्थना करने लगे- ॐ हम भक्षण करें। ॐ हम पान करें। ॐ देव वरुण, प्रजापति, सूर्यदेव यहाँ अन्न लायें हे अन्नपते! यहाँ अन्न लायें, यहाँ अन्न लायें।
तेरहवां खण्ड :
शास्त्रीय संगीत द्वारा साम गायन इस खण्ड में साम सम्बन्धित साधना को शास्त्रीय संगीत की भांति स्वरों का गायन बताया है। इसमें ‘हाउ’ का अर्थ पृथ्वी, ‘हाई’ का अर्थ वायु, ‘अथ’ का अर्थ चन्द्रमा, ‘इह’ का अर्थ आत्मा, ‘ई’ का अर्थ अग्नि, ‘ऊ’ का आदित्य, ‘ए’ का निमन्त्रण, ‘औ होम’ का अर्श विश्वदेवा, ‘हि’ का प्रजापति, ‘स्वर’ प्राण का रूप है, ‘या’ अन्न है और ‘वाक्’ विराट है। इसके अतिरिक्त जो अनिर्वचनीय है और समस्त कार्यों में संचरित होता है, वह तेरहवां स्तोम ‘हुं’ है। जो इस प्रकार साम सम्बन्धी उपनिषद का महत्त्व जानकर उपासना करता है, वह प्रचुर अन्न तथा प्रदीप्त पाचक अग्नि वाला होता है।
द्वितीय अध्याय
दूसरे अध्याय में ‘साम’ को श्रेष्ठता से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में चौबीस खण्ड हैं। इन खण्डों में ‘पंचविध’ और ‘सप्तविध’ साम की उपासना प्रणालियों का वर्णन है।
पहला खण्ड :
साम की पंचविध और सप्तविध उपासनाएं इस खण्ड में साम की सम्पूर्ण उपासना को श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, वह ‘साम’ है। इस प्रकार जो साम की उपासना करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ धर्म की शीघ्र प्राप्ति होती है।
दूसरा खण्ड :
इस खण्ड में साम का भाव साधुतापूर्ण-सदाशयतापूर्ण बताया गया है। ‘उद्गीथ’ ही साम हे। ऊर्ध्व लोकों में पांच प्रकार से साम की उपासना की जाती है। पृथ्वी को ‘हिंकार’, अग्नि को ‘प्रस्ताव,’अन्तरिक्ष को ‘उद्गीथ’ और आदित्य को ‘प्रतिहार’ तथा द्युलोक को ‘निधन’ माना जाता है। इसी प्रकार अधोमुख लोकों में भी पांच प्रकार से साम की उपासना की जाती है। यहाँ स्वर्ग ‘हिंकार’ है, आदित्य ‘प्रस्ताव’ है, अन्तरिक्ष ‘उद्गीथ’ है, अग्नि ‘प्रतिहार’ है और पृथिवी ‘निधन’ है। पंचविध साम की उपासना से ऊर्ध्व और अधोलोकों के समस्त भोग सहज प्राप्त हो जाते हैं।
तीसरा खण्ड :
यहाँ वर्षा में पांच प्रकार से साम की उपासना का वर्णन है। पंचविध साम की उपासना से इच्छानुरूप वर्षा होती है।
चौथा खण्ड :
यहाँ जल में पंचविध साम की उपासना करने वाले की कभी जल में मृत्यु नहीं होती।
पांचवां खण्ड :
यहाँ पर ऋतुओं में पंचविध साम की उपासना करने वाले उपासक को ऋतुएं अभीष्ट फल प्रदान करती हैं।
छठा खण्ड :
इस खण्ड में कहा गया है कि जो पुरुष पशुओं में साम की पंचविध उपासना करता है, उसे भरपूर पशु-सम्पदा प्राप्त होती है।
सातवां खण्ड :
इसी प्रकार प्राणों (इन्द्रियों) में श्रेष्ठता के क्रम से साम की पंचविध उपासना करनी चाहिए। ऐसा करके साधक श्रेष्ठतर जीवन प्राप्त करता है।
आठवां खण्ड :
इस खण्ड में सप्तविध साम की उपासना का वर्णन है। वाणी में ‘हुं’ हिंकार है, शब्द ‘प्र’ प्रस्ताव है, ‘आ’ आदि रूप है, ‘उत्’ उद्गीथ है, ‘प्रति’ प्रतिहार है, ‘उप’ उपद्रव-रूप है और ‘नि’ निधन का रूप है। इस प्रकार जो साधक उपासना से वाणी के सारतत्त्व को प्राप्त कर लेता है, उसे अन्न और अन्न को पचाने की सामर्थ्य प्राप्त होती है।
नौवा खण्ड :
‘आदित्य’ सदा ही सम रहता है। वह साम है। वह सभी के प्रति समभाव वाला है। उदयमान सूर्य ‘प्रस्ताव’ है। सभी मनुष्य और पशु-पक्षी उसके अनुगामी हैं। मध्याह्न में आदित्य ‘उद्गीथ’ है। समस्त देवगण उसके इसी रूप के अनुगामी हैं। उपराह्न में आदित्य ‘प्रतिहार’ है। अस्त होते सूर्य का रूप ही ‘निधन’ हैं आदित्य-रूप साम की इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए।
दसवां खण्ड :
इस खण्ड में आत्मा-तुल्य अतिमृत्यु-रूप की सप्तविध साम की उपासना का वर्णन है। जो साधक परमात्मा-तुल्य अतिमृत्यु-रूप सप्तविध साम की उपासना करता है, वह आदित्य-रूप साम की ही उपासना करता है तथा आदित्यलोक को जीत लेता है।
ग्यारहवां खण्ड :
इस खण्ड में ‘गायत्र’ सम्बन्धी विशिष्ट उपासना का वर्णन है। जो साधक गायत्र-साम को प्राणों में अधिष्ठित हुआ जानता है, वह प्राणवान होता है और पूर्ण आयु को भोगता है।
बारहवां खण्ड :
जो साधक साम को अग्नि में प्रतिष्ठित जानकर उपासना करता है, वह ब्रह्मतेज से सम्पन्न प्रदीप्त जठराग्नि से युक्त होता है। वह पूर्ण तेजोमय जीवन व्यतीत करता है तथा महान कीर्ति को प्राप्त करता है।
तेरहवां खण्ड :
इस खण्ड में स्त्री-पुरुष के जोड़े के रूप मं वामदेव्य साम की उपासना की गयी है। जो साधक दाम्पत्य-जीवन के अनुसार साम की उपासना करता है, वह सन्तति-सुख को प्राप्त करता है।
चौदहवां खण्ड :
यहाँ पुन: उदीयमान सूर्य, उदित हुआ सूर्य तथा अस्त होने वाले सूर्य की साम उपासना का वर्णन है। जो ऐसा जानकर उपासना करता है, वह प्रखर सूर्य की तेजस्विता को प्राप्त करता है।
पन्द्रहवां खण्ड :
वर्षा (पर्जन्य) के साम-रूप की उपासना से साधक विरूप और सुरूप पशुओं का स्वामी होता है और पूर्ण आयु को भोगता है। अत: बरसते मेघों की कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए। जाने आपने भविष्य के बारे में : Astrology in Hindi
सोलहवां खण्ड :
वसन्त ऋतु में वैराज साम को अधिष्ठित मानकर उपासना करने से सुसन्तति, पशु-सम्पदा और ब्रह्मतेज प्राप्त होता है। अत: ऋतुओं की कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए।
सत्रहवां खण्ड :
समस्त लोकों में साम को अधिष्ठित मानकर उपासना करने वाला लोक-विभूतियों से सुशोभित होता है।
अठारहवां खण्ड
रेवती साम को पशुओं में अधिष्ठित मानकर उपासना करने वाला पशु-सम्पदा से समृद्ध होता है।
उन्नीसवां खण्ड :
जो साधक यज्ञीय साम को अंगों सन्निहित जानता है, वह सम्पूर्ण अंगों से स्वस्थ व सम्पन्न होता है।
बीसवां खण्ड :
जो साधक राजन साम को देवताओं में प्रतिष्ठित जानता है, वह उन्हीं देवों के लोकों का ऐश्वर्य और एकरूपता को प्राप्त करता है। अत: ब्राह्मणों की कभी निन्दा नहीं करनी चाहिए।
इक्कीसवां खण्ड :
त्रयी वेद- ॠग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद- के अग्नि, वायु और आदित्य, तीन उद्गीथ हैं, जो साधक इस साम को सम्पूर्ण जगत में प्रतिष्ठित मानता है, वह सर्वरूप हो जाता है।
बाईसवां खण्ड :
अग्निदेव, वायुदेव और इन्द्रदेव के उद्गान अत्यन्त मधुर हैं। समस्त स्वर इन्द्रदेव की आत्मा हैं। सभी स्वर घोषपूर्वक और बलपूर्वक उच्चारण किये जाने चाहिए और मृत्युदेव से अपने को छुड़ाने की प्रार्थना करनी चाहिए।
तेईसवां खण्ड :
यहाँ धर्म के तीन स्कन्धों के विषय में वर्णन किया गया है। धर्म के ये तीन आधारस्तम्भ हैं- यज्ञ, अध्ययन और दान, तप, साधनारत ब्रह्मचारी जब अपने शरीर को क्षीण कर लेता है। प्रथम तीन से त्रयी विद्या-ऋक्, साम और यजु- की उत्पत्ति हुई। दूसरे तप के प्रभाव से त्रयी विद्या से ‘भू:’ और ‘स्व:’ की उत्पत्ति हुई है तथा तीसरे साधना से तीन अक्षरों का सारतत्त्व ओंकार (ॐ) प्राप्त हुआ। ओंकार द्वारा सम्पूर्ण वाणियां व्याप्त हैं। ओंकार ही सम्पूर्ण जगत है और यही सम्पूर्ण आकाश है।
चौबीसवां खण्ड :
यज्ञ के तीन काल इस खण्ड में यज्ञ के तीन-प्राप्त:, मध्याह्न और सांय- सवनों के माध्यम से जीवन के तीन कालों में किये गये साधनात्मक पुरुषार्थ का उल्लेख है।
ब्रह्मवादी कहते हैं कि प्रात:काल का सवन वसुगणों का है, मध्याह्न का रुद्रगणों का और सन्ध्या का आदित्यगणों का तथा विश्वदेवों का है। प्रात:काल यजमान गार्हयत्याग्नि के पीछे उत्तराभिमुख बैठकर वसुदेवों के साम का गान करता है-‘हे अग्निदेव!आप हमें लौकिक सम्पदा प्रदान करें, आप हमें यह लोक प्राप्त करायें। आप हमें मृत्यु के पश्चात पुण्यलोक को प्राप्त करायें।’
इस प्रकार यजमान स्वर्ग, अन्तरिक्ष, अन्तरिक्ष की विभूतियां तथा पुण्यलोक की प्राप्ति की कामना करता है। यही यजमानलोक है। स्वर्गलोक की प्राप्ति हेतु सभी सीमाओं को प्राप्त करने की प्रार्थना यजमान करता है और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के अनुरूप ज्ञान और प्रेरणा का संचार करता है।
तृतीय अध्याय
इस अध्याय में ‘आदित्य’ को ही परब्रह्म मानकर विविध रूपकों द्वारा उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 19 खण्ड हैं।
पहले से पांचवें खण्ड तक :
आदित्य ही परब्रह्म है इन पांच खण्डों में आदित्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम व उत्तर भागों तथा उर्ध्व में स्थित रसों की व्याख्या मधुमक्खियों के छत्ते के रूपक द्वारा की गयी है। ऋषि का कहना है कि सूर्य के समस्त दृश्य, स्थूल रंगों (सप्तरंग) के साथ सूक्ष्म चेतना प्रवाह से जुड़े हैं। ‘ॐकार’ रूप यह आदित्य ही देवों का मधु है। समस्त वेदों- ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेवेद- की ऋचाएं ही मधुमक्खियां हैं, चारों वेद पुष्प हैं और सोम ही अमृत-रूप जल है। इस ब्रह्माण्ड में आदित्य की जो दृश्य प्रक्रिया चल रही हे, उसके पीछे चैतन्य का संकल्प अथवा आदेश ही कार्य कर रहा है।
छठे खण्ड से दसवें खण्ड तक :
इन खण्डों में सूर्य के उन्हीं भागों से अमृत-प्रवाहों के प्रकट होने तथा उसके प्रवाह का वर्णन किया गया है। ऋषि का कहना है कि वसुओं द्वारा प्रवाहित अमृत-तत्त्व को साधकों के मन में स्थित वसु ही जान पाते हैं। उपनिषदों के मत में विराट चेतना में स्थित देवों के अंश मनुष्य के भीतर भी स्थित हैं। अत: वे अपने समानधर्मी प्रवाहों से साधना द्वारा सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं और अमृत का पान करते हैं।
देवगण न तो खाते हैं, न पीते हैं। वे केवल इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। छठे से दसवें खण्ड तक सूर्य के उदय एवं अस्त होने की प्रक्रिया में विभिन्न दिशाओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ उन विभिन्न दिशाओं से विशिष्ट अमृत-प्रवाहों के प्रकट होने की बात कही गयी है। यह अमृत-प्रवाह सूर्य की रश्मियों द्वारा साधक के अन्तर्मन तक प्रवाहित होता है और साधक उस परम सत्ता के ज्योतिर्मय स्वरूप को आत्मसात करता है।
ग्यारहवां खण्ड :
ब्रह्मज्ञान किसे देना चाहिए?
इस खण्ड में ऋषि ‘ब्रह्मज्ञान’ को सुयोग्य शिष्य को ही प्रदान करने की बात कहते हैं। जो साधक ‘ब्रह्मज्ञान’ के निकट पहुंच चुका है अथवा उसमें आत्मसात हो चुका है, उसके लिए सूर्य या ब्रह्म न तो उदित होता है, न अस्त होता है। वह तो सदा दिन के प्रकाश की भांति जगमगाता रहता है और साधक उसी में मगन रहता है।
8किसी समय यह ‘ब्रह्मा जी ने प्रजापति से कहा था। देव प्रजापति ने इसे मनु से कहा और मनु ने इसे प्रजा के लिए अभिव्यक्त किया। उद्दालक ऋषि को उनके पिता ने अपना ज्येष्ठ और सुयोग्य पुत्र होने के कारण यह ब्रह्मज्ञान दिया था। अत: इस ब्रह्मज्ञान का उपदेश अपने सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र अथवा शिष्य को ही देना चाहिए।
बारहवां खण्ड :
गायत्री ही दृश्यमान जगत है
इस खण्ड में ‘गायत्री’ को सब दृश्यमान जगत अथवा भूत माना हैं जगत में जो कुछ भी प्रत्यक्ष दृश्यमान है, वह गायत्री ही है। ‘वाणी’ ही गायत्री है और वाणी ही सम्पूर्ण भूत-रूप है। गायत्री ही सब भूतों का गान करती है और उनकी रक्षा करती है। गायत्री ही पृथ्वी है, इसी में सब भूत अवस्थित हैं यह पृथ्वी भी ‘प्राण-रूप’ गायत्री है, जो पुरुष के शरीर में समाहित है। ये प्राण पुरुष के अन्त:हृदय में स्थित हैं।
गायत्री के रूप में व्यक्त परब्रह्म ही वेदों में वर्णित मन्त्रों में स्थित है। यहाँ उसी की महिमा का वर्णन किया गया है, परन्तु वह विराट पुरुष उससे भी बड़ा है। यह प्रत्यक्ष जगत तो उसका एक अंश मात्र है। उसके अन्य अंश तो अमृत-स्वरूप प्रकाशमय आत्मा में अवस्थित हैं।
वह जो विराट ब्रह्म है, वह पुरुष के बहिरंग आकाश रूप में स्थित है और वही पुरुष के अन्त:हृदय के आकाश में स्थित है। यह अन्तरंग आकाश सर्वदा पूर्ण, अपरिवर्तनीय, अर्थात नित्य है। जो साधक इस प्रकार उस ब्रह्म-स्वरूप को जान लेता है, वह सर्वदा पूर्ण, नित्य और दैवीय सम्पदाएं (विभूतियां) प्राप्त करता है।
तेरहवें खण्ड से उन्नीसवें खण्ड तक :
आदित्य (ब्रह्म) दर्शन अन्त:हृदय में किया जा सकता है। इन खण्डों में ‘आदित्य’ को ही ‘ब्रह्म’ स्वीकार किया गया है और उसकी परमज्योति को ही ब्रह्म-दर्शन माना गया है। इस ज्योति-दर्शन के पांच विभाग भी बताये गये हैं। यह ब्रह्म-दर्शन मनुष्य अपने हृदय में ही कर पाता है। उस अन्त:हृदय के पांच देवों से सम्बन्धित पांच विभाग हैं-
पूर्ववर्ती विभाग- प्राण, चक्षु, आदित्य, तेजस् और अन्न।
दक्षिणावर्ती विभाग- व्यान, श्रोत्र, चन्द्रमा, श्रीसम्पदा और यश।
पश्चिमी विभाग- अपान, वाणी, अग्नि, ब्रह्मतेज और अन्न।
उत्तरी विभाग- समान, मन, पर्जन्य, कीर्ति और व्युष्टि (शारीरिक आकर्षण)।
ऊर्ध्व विभाग- उदान, वायु, आकाश, ओज और मह: (आनन्द तेज)।
जो साधक इस प्रकार जानकर इनकी उपासना करता है, वह ओजस्वी और महान तेजस्वी होता है। स्वर्गलोक के ऊपर जो ज्योति प्रकाशित होती है, वही सम्पूर्ण विश्व में सबके ऊपर प्रकाशित होती है वही पुरुष की अन्त:ज्योति है, अन्तश्चेतना है।
यह सम्पूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्मस्वरूप है। यह उसी से उत्पन्न होता है और उसी में लय हो जाता है तथा उसी के द्वारा संचालित होता है। राग-द्वेष से रहित होकर ही शान्त भाव से इसकी उपासना करनी चाहिए।यह पुरुष् ही यज्ञ है और प्राण ही वायु हैं। ये सभी को आवास देने वाले हैं। जो भोगों में लिप्त नहीं होता, वही उसकी दीक्षा है।
अंगिरस ऋषि ने देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण को तत्त्वदर्शन का उपदेश दिया थां उससे वे सभी तरह की पिपासाओं से मुक्त हो गये थे। साधक को मृत्युकाल में तीन मन्त्रों का स्मरण करना चाहिए-(तध्दैत्दघोर आगिंरस कृष्ण्णाय देवकीपुत्रायोक्त्वोवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रय प्रतिपद्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राण्सँशितमसीति तत्रैते द्वे ॠचौ भवत: ॥)
मृत्युकाल के तीन मन्त्र :
तुम अक्षय, अनश्वर-स्वरूप हो, तुम अच्युत-अटल, पतित न होने वाले हो तथा तुम अतिसूक्ष्म प्राणस्वरूप हो। ब्रह्मज्ञानी अन्धकार (अज्ञान) से निकलकर परब्रह्म के प्रकाश को देखते हुए और आत्म-ज्योति में ही देदीप्यमान सूर्य की सर्वोत्तम ज्योति को प्राप्त करता है। यह मन ही ब्रह्म-स्वरूप है। हमें इसी की उपासना करनी चाहिए।
मनोमय ब्रह्म के चार पाद (चरण)। मनोमय ब्रह्म के चार पाद हैं- वाणी, प्राण, चक्षु और श्रोत्र। इनके द्वारा ही साधक मनोमय ब्रह्म की दिव्य ज्योति का दर्शन कर पाता है, उसके आनन्दमय स्वरूप को अनुभव कर पाता है तथा उसकी आदित्य-रूप ज्योति से दीप्तिमान होकर तेजस्वी हो पाता है।
‘आदित्य’ ही ब्रह्म है। जो यह जानकर उपासना करता है, उसके समीप सुखप्रद ‘नाद’ सुनाई देता है और वह नाद ही उसे सुख तथा सन्तोष प्रदान करता है। आदिकाल में यह आदित्य अदृश्य रूप में था। बाद में यह सतरूप (प्रत्यक्ष) में प्रकट हुआ। वह विकसित होकर अण्डे के रूप में परिवर्तित हुआ। कालान्तर में वह अण्डा विकसित हुआ और फूटा। उसके दो खण्ड हुए- एक रजत और एक स्वर्ण। रजत खण्ड पृथ्वी है और स्वर्ण खण्ड द्युलोक (अन्तरिक्ष) है। उस अण्डे से जो उत्पन्न हुआ, वह आदित्य ही है। यही आदित्य ‘ब्रह्म’ है।
चतुर्थ अध्याय
इस अध्याय में सत्रह खण्ड हैं प्रथम तीन खण्डों में राजा जनश्रुति और गाड़ीवान रैक्व का संवाद है। उन संवादों के माध्यम से रैक्व राजा जनश्रुति को ‘वायु’ और ‘प्राण’ की श्रेष्ठता के विषय में बताता है।
चतुर्थ से नवम खण्ड तक जाबाला-पुत्र सत्यकाम की कथा है, जिसमें वृषभ, अग्नि, हंस और जल पक्षी के माध्यम से ‘ब्रह्म’ का उपदेश दिया गया है और दशम से सत्रहवें खण्ड तक सत्यकाम जाबाल के शिष्य उपकोसल को विभिन्न अग्नियों द्वारा तथा अन्त में आचार्य सत्यकाम द्वारा ‘ब्रह्मज्ञान’ दिया गया है तथा यज्ञ का ब्रह्मा कौन है, इस ओर संकेत किया है।
एक से तीसरे खण्ड तक :
एक बार प्रसिद्ध राजा जनश्रुति के महल के ऊपर से दो हंस बातें करते हुए उड़े जा रहे थे। यद्यपि राजा के महल से ‘ब्रह्मज्ञान’ का तेज प्रकट हो रहा था, तथापि हंसों की दृष्टि में वह तेज इतना तीव्र नहीं था, जितना कि गाड़ीवान रैक्व का था।
राजा ने हंसों की बातें सुनी, तो रैक्व की तलाश करायी गयी। बड़ी कठिनाई से रैक्व मिला। राजा अनेक उपहार लेकर उसके पास गया, पर उसने ‘ब्रह्मज्ञान’ देने से मना कर दिया। राजा दूसरी बार अपनी राजकुमारी को लेकर रैक्व के पास गया। रैक्व ने राजकन्या का आदर रखने के लिए राजा को ‘ब्रह्मज्ञान’ दिया।
‘हे राजन! देवताओं में ‘वायु’ और इन्द्रियों में ‘प्राण’ ये दो ही संवर्ग (अपनी ओर खींचकर भक्षण करना) हैं। इन्हें ही ‘ब्रह्मरूप’ समझकर इनकी उपासना करना उत्तम है; क्योंकि अग्नि जब शान्त होती है, तो वह वायु में विलीन हो जाती है। उसी प्रकार जल जब सूखता है, तो वुय में समाहित हो जाता है। यही वायु मनुष्य के शरीर में ‘प्राण’ रूप में स्थित है। इसे आधिदैविक उपासना कहते हैं। साधक के सोने पर मनुष्य के शरीर में ‘प्राण’ उसकी समस्त वागेन्द्रियों को अपने भीतर समेट लेता है। प्राण में ही चक्षु, श्रोत्र और मन समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राणवायु ही सबको अपने भीतर समाहित करने वाला है। यही सत्यरूप आध्यात्मिक तत्त्व है।’
चौथे खण्ड से नौवें खण्ड तक :
इन खण्डों के पहले छह खण्डों में जाबाल-पुत्र सत्यकाम की कथा है। एक बार सत्यकाम ने अपनी माता जाबाला से कहा-‘माता! मैं ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना चाहता हूं। मुझे बतायें कि मेरा गोत्र क्या है?’
माता ने उत्तर दिया-‘मैं युवावस्था में विभिन्न घरों में सेविका का कार्य करती थी। वहां किसके संसर्ग से तुम्हारा जन्म हुआ, मैं नहीं जानती, परन्तु मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। अत: तू सत्यकाम जाबाला के नाम से जाना जायेगा।’ सत्यकाम ने हारिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा-‘हे भगवन! मैं आपके पास ब्रह्मचर्य के साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ।’ गौतम ने जब उससे उसका गोत्र पूछा, तो उसने अपने जन्म की साफ-साफ कथा बता दी। गौतम उसके सत्य से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे चार सौ गौंए देकर चराने के कार्य पर लगा दिया।
साथ ही यह भी कहा कि जब एक हज़ार गौएं हो जायें, तब वह आश्रम में लौटे। सत्यकाम वर्षों तक उन गौओं के साथ वन में भ्रमण करता रहा। जब एक हज़ार गौएं हो गयीं, तब एक वृषभ ने उससे कहा-‘सत्यकाम! तुमने इतनी गौ-सेवा की है, अत: तुम ब्रह्म के चार पदों को जानने योग्य हो गये हो। देखो, यह पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व उत्तर दिशा ‘प्रकाशमान ब्रह्म’ की चार कलाएं हैं। वह ‘प्रकाशवान ब्रह्म’ इन चारों कलाओं में एक पाद है। इस प्रकार जानने वाला साधक ब्रह्म के प्रकाशवान स्वरूप की उपासना करता है। अब ब्रह्म के दूसरे पाद के बारे में तुम्हें अग्निदेव बतायेंगे।’
सत्यकाम गौएं लेकर गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिया। मार्ग में उसने अग्नि प्रज्वलित की। तब अग्नि ने कहा-‘सत्यकाम! अनन्त ब्रह्म की- पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक और समुद्र- चार कलाएं हैं। हे सौम्य! ब्रह्म का दूसरा पाद ‘अनन्त ब्रह्म’ है। अब ब्रह्म के तीसरे पाद के विषय में तुम्हें हंस बतायेगा।’ दूसरे दिन सत्यकाम गौओं को लेकर आचार्यकुल की ओर चल पड़ा। सांयकाल वह रूका और अग्नि प्रज्वलित की, तो हंस उड़कर वहां आया और बोला-‘हे सत्यकाम! अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत, ब्रह्म की ये चार कलाएं हैं। ब्रह्म का तीसरा पाद यह ‘ज्योतिष्मान’ है। जो ज्योतिष्मान संज्ञक चतुष्कल पाद की उपासना करता है, वह इसी लोक में यश और कीर्ति को प्राप्त करता है।
अब चौथे पद के बारे में तुम्हें जल-पक्षी बतायेगा।’ अगले दिन वह आचार्यकुल की ओर आगे बढ़ा, तो सन्ध्या समय जल-पक्षी उसके पास आकर बोला-‘सत्यकाम! प्राण, चक्षु, कान और मन, ब्रह्म की चार कलाएं हैं। ब्रह्म का चतुष्काल पाद यह आयतनवान (आश्रयमयुक्त) संज्ञक हैं इस आयतनवान संज्ञक की उपासना करने वाला विद्वान ब्रह्म के इसी रूप को प्राप्त कर लेता है।’ जब सत्यकाम आचार्यकुल पहुंचा, तो आचार्य गौतम ने उससे कहा-‘हे सौम्य! तुम ब्रह्मवेत्ता के रूप में दीप्तिमान हो रहे हो। तुम्हें किसने उपदेश दिया?’ सत्यकाम ने बता दिया और उनसे उपदेश पाने की कामना की। तब आचार्य ने सत्यकाम को उपदेश दिया-‘हे सत्यकाम! भगवद्-स्वरूप ऋषियों के मुख से जानी गयी विद्या ही उपयुक्त सार्थकता को प्राप्त होती है।’
दसवें खण्ड से सत्रहवें खण्ड तक :
अग्नियों द्वारा ब्रह्मज्ञान का उपदेश गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सत्यकाम आचार्यपद पर आसीन हो गये। तब उन्होंने अपने शिष्य उपकोसल को विभिन्न अग्नियों का उदाहरण देकर ‘ब्रह्मज्ञान’ का उपदेश-दिया। कमल का पुत्र उपकोसल ब्रह्मचर्यपूर्वक बारह वर्ष तक सत्यकाम जाबाल के पास रहकर अग्नियों की सेवा में लाभ रहा। दीक्षा समाप्त होने पर सत्यकाम ने सभी शिष्यों को दीक्षा दी, पर उपकोसल को नहीं दीं इस पर उपकोसल निराश होकर भोजन त्याग का निर्णन कर बैठा। इस पर अग्नियों ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि वे उपकोसल को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देंगी।
अग्नियों ने कहा-‘उपकोसल वत्स! प्राण ही ब्रह्म है। ‘क’ (सुख) ब्रह्म है और ‘ख’ (आकाश) भी ब्रह्म है। प्राण का आधार आकाश है। पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य, इन चारों में मैं ही हूं। आदित्य के मध्य जो पुरुष दिखाई देता है, वह मैं हूं। वही मेरा विराट रूप है। जो पुरुष इस प्रकार जानकर उस आदित्य पुरुष की उपासना करता है, वह पापकर्मों को नष्ट कर देता है। वह अग्नि के समस्त भोगों को प्राप्त करता है तथा पूर्ण आयु और तेजस्वी जीवन जीता है।’ इसके बाद आहवनीय अग्नि ने प्राण, आकाश, द्युलोक और विद्युत में अपनी उपस्थिति बतायी और कहा-‘हे सौम्य! हमने तुझे आत्म-विद्या का ज्ञान कराया। अब आचार्य तुझे आगे बतायेंगे।’
आचार्य सत्यकाम ने सबसे अन्त में उपकोसल से कहा-‘हे वत्स! इन अग्नियों ने तुम्हें केवल लोकों का ज्ञान दिया है। अब मैं तुम्हें पापकर्मों को नष्ट करने वाला ज्ञान देता हूं। उपकोसल! नेत्रों में जो यह पुरुष दिखाई देता है, यही आत्मा हे। यह अविनाशी, भयरहित और ब्रह्मस्वरूप है। सम्पूर्ण शोभन और सर्वोपयोगी वस्तुएं यही धारण करता है और साधक को पुण्यकर्मों का फल प्रदान करता है। यह पुरुष निश्चय ही प्रकाशमान है व सम्पूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाला है। जब मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, तब अज्ञान का अन्धकार मिट जाता है और साधक अपने मन में परब्रह्म के दर्शन करता है।’
तान्त्रिक मतानुसार दोनों भौंहों के मध्य आज्ञचक्र स्थित है, जहां ध्यान लगाने पर ‘ओंकार’ स्वरूप प्रणव ब्रह्म का दर्शन होता है। यह प्रवहमान वायु ही यज्ञ है। यह सम्पूर्ण जगत को पवित्र करता है। ‘वाणी’ और ‘मन’ इसके दो मार्ग हैं। एक मार्ग का संस्कार ब्रह्मा अपने मन से करता है, दूसरे का होता अपनी वाणी से करता है। ऐसा यज्ञ करके यजमान विशेष श्रेय का अधिकारी हो जाता है।
यज्ञ का ब्रह्म कौन है?
अन्त में, प्रजापति ब्रह्मा तप करके लोकों का रसतत्त्व उत्पन्न करता हैं। पृथ्वी से अग्नि, अन्तरिक्ष से वायु और द्युलोक से आदित्य को ग्रहण करता है। अग्नि से ऋक्, वायु से यजुष और आदित्यदेव से साम को ग्रहण करता है। ऋचाओं से ‘भू:’ यजु:, कण्डिकाओं से ‘भुव:’ तथा साम मन्त्रों से ‘स्व:’ को ग्रहण करता है।
- यदि ऋचाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो, तो ‘भू: स्वाहा’ कहकर यज्ञ करें।
- यदि यजु: कण्डिकाओं के यज्ञ में कोई त्रुटि हो, तो ‘भुव: स्वाहा’ कहकर यज्ञ करें।
- यदि साम मन्त्रों के यज्ञ में कोई त्रुटि हो तो, ‘स्व: स्वाहा’ कहकर यज्ञ करें।
जिस यज्ञ में ब्रह्मा ऋत्विक होता है, वहां वह यज्ञ की, यजमान की और समस्त ऋत्विजों की सब ओर से रक्षा करता है। इस प्रकार श्रेष्ठ ज्ञानवान को ही यज्ञ का ब्रह्मा बनाना चाहिए।
पंचम अध्याय
इस अध्याय में ‘प्राण’ की सर्वश्रेष्ठता एवं पंचाग्नि विद्या का विशद वर्णन किया गया है। साथ ही अग्नि का महत्त्व, जीव की गति, ‘आत्मा’ पर सत्यकाम जाबाल, श्वेतकेतु और प्रवाहण का संवाद तथा जीवन-जगत के गूढ़तम विषयों का सरल भाष्य प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में चौबीस खण्ड हैं।
प्रथम खण्ड :
शरीर में प्राणतत्त्व की सर्वश्रेष्ठता इस शरीर में जो स्थान ‘प्राण’ का है, वह किसी अन्य इन्द्रिय का नहीं है। एक बार सभी इन्द्रियों में अपनी-अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया। तब सभी ने प्रजापति ब्रह्मा से निर्णय जानना चाहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? इस पर प्रजापति ने कहा कि तुमसें से जिसके द्वारा शरीर छोड़ देने पर वह निश्चेष्ट हो जाये, वही श्रेष्ठ है।
सबसे पहल वाणी ने, उसके बाद चक्षु ने, फिर कानों ने, फिर मन ने शरीर को बारी-बारी से छोड़ा, किन्तु हर बार शरीर का एक अंग ही निश्चेष्ट हुआ। शेष शरीर सक्रिय बना रहा। जैसे वाणी के जाने से वह गूंगा हो गया, चक्षु के जाने से अन्धा हो गया, कानों के जाने से बहरा हो गया और मन के जाने से बालक-रूप-जैसा हो गया, पर जीवित रहा और अपने सारे कार्य करता रहा, किन्तु जब ‘प्राण’ जाने लगा, तो सारी इन्द्रियाँ शिथिल होने लगीं। उन्होंने घबराकर प्राण को रोका और उसकी सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया।
दूसरा खण्ड :
महानता के लिए ‘मन्थ’ अनुष्ठान इस खण्ड में ‘मन्थ’ अनुष्ठान का वर्णन है। प्राण ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के उपरान्त पूछा- ‘मेरा भोजन क्या होगा?’ अन्य इन्द्रियों ने उत्तर दिया-‘अन्न’ तुम्हारा भोजन होगा। प्राण ने फिर पूछा- ‘मेरा वस्त्र क्या होगा? इन्द्रियों ने उत्तर दिया ‘जल तुम्हारा वस्त्र होगा।’ यह ज्ञान सत्यकाम जाबाल ने अपने शिष्य व्याघ्नपद के पुत्र गोश्रुति नामक व्याघ्नपद को सुनाया था। तदुपरान्त यदि कोई महत्त्व प्राप्त करने का अभिलाषी हो, तो उसे अमावस्या की दीक्षा प्राप्त करके पूर्णिमा की रात्रि को सभी औषधियों, दही और शहद सम्बन्धी ‘मन्थ’ (मथकर तैयार किया हुआ हव्य) का मन्थन करके जेष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा के मन्त्र द्वारा अग्नि में घृत की आहुति देकर ‘मन्थ’ में उसका अवशेष डालना चाहिए।
इसी प्रकार वसिष्ठाय स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा, सम्पदे स्वाहा और आयतनाम स्वाहा मन्त्रों से अग्नि में घी की आहुति देकर शेष घी को ‘मन्थ’ में छोड़े। तत्पश्चात अग्नि से कुछ दूर हटकर अंजलि में ‘मन्थ’ को लेकर अमो नामसि (हे मन्थ! तू अम, अर्थात प्राण है, सम्पूर्ण जगत तेरे साथ है, तू ही ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, प्रकाशमान और सबका अधिपति है।) मन्त्र पढ़कर आचमन करें। उसके बाद भोजन की प्रार्थना करें तत्त्सवितुर्वृणीमहे, वयं देवस्य भोजनम्, श्रेष्ठं सर्वधातमम् और तुंरभगस्य धीमहि मन्त्रों को कहते हुए मन्थ का एक-एक ग्रास भक्षण करे और अन्त में बरतन को धोकर सम्पूर्ण ‘मन्थ’ को पी जाये। इसके बाद अग्नि के उत्तर में पवित्र मृगचर्म बिछाकर शयन करे। यदि उस रात स्वप्न में किसी स्त्री का दर्शन हो, तो समझे कि अनुष्ठान पूरा और सफल हो गया।
तीसरे खण्ड से दसवें खण्ड तक :
अग्नि उपासना तथा देवयान और पितृयान मार्ग
इन खण्डों में अग्नि की उपासना के महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है और देवयान मार्ग तथा पितृयान मार्ग के मर्म को समझाया गया है। ये दोनों मार्ग, मृत्यु, के पश्चात जीव (आत्मा) जिन मार्गों से ब्रह्मलोक जाता है, उन्हीं के विषय को दर्शाते हैं। ये दोनों मार्ग भारतीय आपनिषदिक दर्शन की विशिष्ट संकल्पनाएं हैं। इनका उल्लेख ‘कौषीतकि’ और ‘बृहदारण्यक’ उपनिषदों में भी विस्तार से किया गया है।
एक बार आरुणि-पुत्र श्वेतकेतु पांचाल नरेश जीवल की राजसभा में पहुंचा। जीवल के पुत्र प्रवाहण ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की है? इस पर श्वेतकेतु ने ‘हां’ कहां तब प्रवाहण ने उससे कुछ प्रश्न किये-प्रवाहण-‘क्या तुम्हें पता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा कहां जाती है? क्या तुम्हें पता है कि वह आत्मा इस लोक में किस प्रकार आती है? क्या तुम्हें देवयान और पितृयान मार्गों के अलग होने का स्थान पता है? क्या तुम्हें पता है कि पितृलोक क्यों नहीं मरता? क्या तुम्हें पता है कि पांचवीं आहुति के यजन कर दिये जाने पर घृत सहित सोमादि रस ‘पुरुष’ संज्ञा को कैसे प्राप्त करते हैं?’ प्रवाहण के इन प्रश्नों का उत्तर श्वेतकेतु ने नकारात्मक दियां तब प्रवाहण ने कहा-‘फिर तुमने क्यों कहा कि तुम्हें शिक्षा प्रदान की गयी है?’
श्वेतकेतु इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे सका। वह त्रस्त होकर अपने पिता के पास आया और उन्हें सारा वार्तालाप सुनाया। आरुणि ने भी उन प्रश्नों का उत्तर न जानने के बारे में कहा। तब दोनों पिता-पुत्र पांचाल नरेश जीवल के दरबार में पुन: आये और प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा प्रकट की। राजा ने दोनों का स्वागत किया और कुछ काल अपने यहाँ रखकर एक दिन कहा-‘हे गौतम! प्राचीनकाल में यह अग्नि-विद्या ब्राह्मणों के पास नहीं थी। इसी कारण यह विद्या क्षत्रियों के पास रही।’राजा ने आगे कहा-‘हे गौतम! यह प्रसिद्ध द्युलोक ही अग्नि है। आदित्य अग्नि का ईधन है, किरणें धुआं हैं, शदिन ज्वाला है, चन्द्रमा अंगार है और नक्षत्र चिनगारियां हैं इस द्युलोक अग्नि में देवगण श्रद्धा से यजन करते हैं। वे जो आहुति डालते हैं, उससे ‘सोम’ राजा का प्रादुर्भाव होता है।’
राजा ने आगे कहा-‘हे गौतम! इस अग्नि-विद्या में पर्जन्य ही अग्नि है। वायु समिधाएं हैं, बादल धूम्र हैं, विद्युत ज्वालाएं है, वज्र अंगार है और गर्जन चिनगारियां हैं। इस देवाग्नि में सोम की आहुति डालने से वर्षा प्रकट होती है।’ राजा ने फिर कहा-‘हे गौतम! पृथ्वी ही अग्नि है, संवत्सर समिधाएं हैं, आकाश धूम्र है, रात्रि ज्वालाएं हैं, दिशाएं अंगारे हैं और उनके कोने चिनगारियां हैं। उस श्रेष्ठ दिव्याग्नि में वर्षा की आहुति पड़ने से अन्न् का प्रादुर्भाव होता है।’ राजा ने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया-‘हे गौतम! यह पुरुष ही दिव्याग्नि है, वाणी समिधाएं हैं, प्राण धूम्र है, जिह्वा ज्वाला है, नेत्र अंगारे हैं और कान चिनगारियां हैं। इस दिव्याग्नि में सभी देवता मिलकर जब अन्न की आहुति देते हैं, तो वीर्य, अर्थात पुरुषार्थ की उत्पत्ति होती है।’
पांचवें प्रश्न का उत्तर देते हुए राजा ने कहा-‘हे गौतम!उस अग्नि-विद्या की स्त्री ही दिव्याग्नि है, उसका गर्भाशय समिधा है, विचारों का आवेग धुआं है, उसकी योनि ज्वाला है, स्त्री-पुरुष के सहवास से उत्पन्न दिव्याग्नि अंगारे हैं और आनन्दानुभूति चिनगारियां हैं उस दिव्याग्नि में देवगण जब वीर्य की आहुति डालते हैं, तब श्रेष्ठ गर्भ का अवतरण होता है। इस पांचवीं आहुति के उपरान्त प्रथम आहुति में होमा गया ‘आप:’ (जल-मूल जीवन) काया में स्थित पुरुषवाचक ‘जीव या प्राणी’ के रूप में विकसित हो जाता है।
‘समय आने पर यही जीव, जीवन-प्रवाह में पड़कर नया जन्म ले लेता है और निश्चित आयु तक जीवित रहता है। इसके बाद शरीर त्यागने पर कर्मवश परलोक को गमन करते हुए वह वहीं चला जाता है, जहां से वह आया था। जो साधक इस पंचग्नि-विद्या को जानकर श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं, वे सभी प्राणी, प्रयाण के उपरान्त ‘देवयान मार्ग’ और ‘पितृयान मार्ग’ से पुन: द्युलोक में चले जाते हैं।’
देवयान और पितृयान मार्ग :
‘देवयान मार्ग’ के अन्तर्गत प्राणी मृत्यु के उपरान्त अग्निलोक या प्रकाश पुंज रूप से दिन के प्रकाश में समाहित हो जाते हैं। चन्द्रमा के शुक्ल पक्ष से वे उत्तरायण सूर्य में आ जाते हैं। छह माह के इस संवत्सर को आदित्य में, आदित्य को चन्द्रमा में, चन्द्रमा को विद्युत में, विद्युत को ब्रह्म में पुन: समाहित होने का अवसर प्राप्त होता है। इसे ही आत्मा के प्रयाण का ‘देवयान मार्ग’ कहा जाता है। इस मार्ग से जाने वाले जीव का पुनर्जन्म नहीं होता।
‘पितृयान मार्ग’ से वे प्राणी मृत्यु के उपरान्त जाते हैं, जिन्हें ब्रह्मज्ञान किंचित मात्रा में भी नहीं होता। वे लोग धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। धुएं के रूप में वे रात्रि में गमन करते हैं। रात्रि से कृष्ण पक्ष में और कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन सूर्य में समाहित हो जाते हैं। ये लोग देवयान मार्ग से जाने वाले जीवों की भांति संवत्सर को प्राप्त नहीं होते। ये दक्षिणायन से पितृलोक आकाश में और आकाश से चन्द्रमा में चले जाते हैं। इससे आगे वे ब्रह्म को प्राप्त नहीं होते।
अपने कर्मों का पुण्य क्षय होने पर ये आत्माएं पुन: वर्षा के रूप में मृत्युलोक में लौट आती है। ये उसी मार्ग से वापस आती हैं, जिस मार्ग से ये चन्द्रमा में गयी थीं। वर्षा की बूंदों के रूप में जब ये पृथ्वी पर आती हैं, तो अन्न और वनस्पति-औषधियों के रूप में प्रकट होती हैं। तब उस अन्न और वनस्पति का जो-जो प्राणी भक्षण करता है, ये उसी के वीर्य में जीवाणु के रूप में पहुंच जाती हैं पुन: मातृयोनि के द्वारा जन्म लेती हैं।
पितृयान से जाने वाले जीव पुन: जन्म लेते हैं। फिर वह चाहे पशु योनि में आयें, चाहे मनुष्य योनि में। जीवन और मरण का यही रहस्य है।
ग्यारहवें खण्ड से चौबीसवें खण्ड तक :
आत्मा और ब्रह्म का सत्य तथा शरीर से उसका सम्बन्ध
इन खण्डों में राजा अश्वपति और प्राचीनशाल उपमन्यु के पुत्र ‘औपमन्यव’, भाल्लवेय वैयाघ्रपय ‘इन्द्रद्युम्न,’पौलुषि-पुत्र ‘सत्ययज्ञ’, शार्कराक्ष-पुत्र ‘जन’, अश्वतराश्व-पुत्र ‘बुडिल’ और अरुण-पुत्र ‘उद्दालक’ के मध्य हुए प्रश्नोत्तर में ‘आत्मा’ और ‘ब्रह्म’ के मर्म को समझाया गया है तथा ब्रह्माण्ड व मानव-शरीर के छ: अंगों की तुलनात्मक व्याख्या की गयी हैं।
एक बार ये छह ऋषि राजा अश्वपति के पास जाकर अपनी शंका का समाधान करते हैं। तब राजा अश्वपति सभी से अलग-अलग प्रश्न करके पूछते हैं कि वे किस ‘आत्मा’ की उपासना करते हैं। ‘औपमन्यव’ ने कहा कि वे ‘द्युलोक’ की उपासना करते हैं, ‘इन्द्रद्युम्न’ ने कहा कि वे ‘वायुदेव’ की उपासना करते हैं, ‘सत्ययज्ञ’ ने कहा कि वे ‘आदित्य’ की उपासना करते हैं, ‘जन’ ने कहा कि वे ‘आकाशतत्त्व’ की उपासना करते हैं, ‘बुडिल’ ने कहा कि वे ‘जलतत्त्व’ की उपासना करते हैं और ऋषिकुमार ‘उद्दालक’ ने कहा कि वे ‘पृथ्वीतत्त्व’ की उपासना करते हैं। इस पर राजा अश्वपति ने ‘औपमन्यव’ ने कहा कि आप जिस द्युलोक की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही ‘सुतेजा’ नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर-रूप आत्मा ही है। आप अन्न का भक्षण करते हैं और अपने प्रिय पुत्र-पौत्रादि को देखते हैं और अपने कुल में ब्रह्मतेज से युक्त होते हैं।
फिर राजा ने ‘इन्द्रद्युम्न’ से कहा कि आप जिस वायुदेव की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही अलग-अलग मार्गों वाला वैश्वानर आत्मा है। यह आत्मा का प्राण है। इसी के प्रभाव से आपके पास भिन्न-भिन्न अन्न-वस्त्र आदि उपहार के रूप में आते हैं तथा आपके पीछे अलग-अलग रथ की श्रेणियां चलती हैं। राजा ने पुन: ‘सत्ययज्ञ’ से कहा कि आप जिस आदित्य की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है। यही कारण है कि आपके वंश में पर्याप्त मात्रा में विश्व-रूप साधक दृष्टिगोचर होते हैं। यह आदित्य आत्मा का ही ‘चक्षु’ है।
इसके अनन्तर राजा ने ‘शार्कराक्ष-पुत्र जन’ से कहा कि आप जिस आकाश-तत्त्व की उपासना करते हैं, वह निश्चय ही विभिन्न संज्ञाओं से युक्त वैश्वानर आत्मा ही है। यह आत्मा ‘उदरय ही है। इसी से आप धन-धान्य और सन्तान पक्ष की ओर से समृद्ध हैं। आत्मा के इस रूप को पहचानकर, जो अन्न का भक्षण तथा प्रिय का दर्शन करता है, उसके कुल में ब्रह्मतेज का निवास होता है।
इसके बाद राजा अश्वपति ने ऋषिकुमार’ बुडिल’ से कहा कि वह जिस जलतत्त्व की उपासना करता है, वह निश्चय ही श्रीसम्पन्न वैश्वानर आत्मा है, किन्तु यह आत्मा ‘मूत्राशय’ का आधार है। अन्त में राजा ने अरुण-पुत्र ‘उद्दालक’ से कहा कि वह जिस पृथ्वीतत्त्व की उपासना करता है, वह निश्चय ही पग-रूप (प्रतिष्ठासंज्ञक) वैश्वानर आत्मा है। इसकी कृपा से उसे प्रजा और पशुओं की प्राप्ति हुई है। ये पग-रूप आत्मा के ‘चरण’ ही है।
इस प्रकार राजा ने छह ऋषियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोग इस वैश्वानर-स्वरूप आत्मा को पृथक्-पृथक् जानते हुए भी अन्न का भक्षण करते हैं जो भी मनुष्य ‘यही मैं हूं’ जानकर अपने अहं का हेतु होने वाले इस प्रदेश, अर्थात ‘द्यु-मूर्धा’ से लेकर ‘पृथ्वी’ पर्यन्त वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है, वह सभी लोकों में, सभी प्राणियों में और सभी आत्माओं में, अन्न का भक्षण करता है।
राजा उपदेश देते हुए कहता है कि इस वैश्वानर आत्मा का ‘मस्तक’ ही ‘द्युलोक’ है, ‘नेत्र’ ही ‘सूर्य’ है, ‘प्राण’ ही ‘वायु’ हैं, शरीर के बीच का भाग ‘आकाश’ है, ‘बस्ति’ (मूत्राशय) ही ‘जल’ है, ‘पृथिवीय दो ‘पैर’ है, ‘वक्ष’ ‘वेदी’ है, ‘रोमकूप’ ही ‘कुश’ है, ‘हृदय’ ही ‘गार्हपत्याग्नि’ है, ‘मन’ ‘दक्षिणाग्नि’ है और ‘मुंह’ ‘आहवनीय अग्नि’ के समान है; क्योंकि अन्न का हवन इसी में होता है।
राजा ने उन्हें समझाया कि आप सभी वैश्वानर आत्मा के एक-एक अंग की उपासना करते थे। किसी एक अंग में स्थित आत्मा की उपासना से ‘आत्मतत्त्व’ की अनुभूति तो की जा सकती है, किन्तु उसे वहीं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। वह तो अनन्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। यदि उस विराट चैतन्य शक्ति को किसी एक अंग तक सीमित रखा जायेगा, तो वह विराट के सतत प्रवाह को बनाये रखने में असफल हो जायेगा। उससे उस अंग-विशेष को हानि हो सकती है। वह अनेकानेक विकारों से ग्रसित हो सकता है।’ब्रह्म’ और ‘मानव-शरीर’ ‘ब्रह्म’ की रचना और ‘मानव-शरीर’ की रचना में गहरा साम्य है। यहाँ इसी तथ्य का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया गया है। पंचतत्वों-
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से ‘मानव-शरीर’ और ‘ब्रह्म’ की रचना का साम्य दर्शाया गया है। ‘द्युलोक’ (आकाश) ब्रह्म का मस्तक है। यहीं आत्मा निवास करती है। ‘आदित्य’ (अग्नि) को ब्रह्म के नेत्र कहा गया है। ‘वायु’ प्राण-रूप में शरीर में स्थित है। ‘जल’ का स्थान उदर या मूत्राशय में है। ‘पृथ्वी’ ब्रह्म के चरण है। इस प्रकार ‘ब्रह्म’ अपने सम्पूर्ण विराट स्वरूप में इस मानव-शरीर में भी विद्यमान है। इस मर्म को समझकर ही साधक को अन्तर्मुखी होकर ‘ब्रह्म’ की उपासना, अपने शरीर में ही करनी चाहिए। ‘ब्रह्म’ इस शरीर से अलग नहीं है। यह ‘आत्मा’ ही ब्रह्म का अंश है।
राजा अश्वपति ने इस रहस्य को समझाते हुए सभी ऋषिकुमारों को यज्ञकर्म करने की प्रेरणा दी और समस्त लोकों तथा प्राणी समुदाय की समस्त आत्माओं के कल्याण के लिए यज्ञकर्म के महत्त्व का प्रतिपादन किया।
यज्ञकर्म कैसे करें?
राजा अश्वपति ने कहा कि ‘पंच प्राण’ व शरीर की विभिन्न कर्मेन्द्रियों का अटूट सम्बन्ध है। यदि वैश्वानर विद्या को अच्छी प्रकार से जानकर यज्ञकर्म किया जाये, तो सभी कर्मेंन्द्रियों में ‘ब्रह्मतेज’ का उदय होना अनिवार्य है।
सर्वप्रथम पकाये हुए भोजन से ‘प्राणाय स्वाहा’ मन्त्र पढ़कर यज्ञ में आहुति दें। इससे ‘प्राण’ तृप्त होते हैं, चक्षुओं के तृप्त होने से सूर्य तृप्त होता है, सूर्य के तृप्त होने से ‘द्युलोक’ (आकाश) तृप्त होता है, द्युलोक के तृप्त होने से स्वयं भोग लगाने वाला साधक, ब्रह्मतेज से तृप्त हो जाता है।
इसी प्रकार दूसरी आहुति, ‘व्यानाय स्वाहा’ मन्त्र पढ़कर ‘व्यान’ को तृप्त करें। व्यान की तृप्ति से कर्मेन्द्रियां तृप्त हो जाती है।
तीसरी आहुति ‘अपानाय स्वाहा’ मन्त्र से दें। इससे ‘अपान’ तृप्त होता है और अपान की तृप्ति से वागिन्द्रिय (वाणी) की तृप्ति होती है।
चौथी आहुति ‘समानाय स्वाहा’ से दें। इससे ‘समान’ तृप्त होता है। और समान की तृप्ति से ‘मन’ तृप्त होता है।
पांचवीं आहुति ‘उदानाय स्वाहा’ से दें। इससे उदान तृप्त होता है और उदान की तृप्ति से ‘त्वचा’ की तृप्ति होती है।
इस प्रकार किये गये यज्ञकर्म से ‘ब्रह्मतेज’ तृप्त होता है और उसके तृप्त होने से सम्पूर्ण पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त आत्माओं और लोकों में ब्रह्मतेज का प्रादुर्भाव हो जाता है।
षष्ठ अध्याय
ब्रह्मऋषि आरुणि-पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को सत्य-स्वरूप ‘ब्रह्म’ को विविध उदाहरणों द्वारा समझाया था और सृष्टि के सृजन की विधिवत व्याख्या की थी। इस अध्याय में उसी का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में सोलह खण्ड हैं ।
पहला और दूसरा खण्ड :
जगत की उत्पत्ति
पहले दो खण्डों में ‘जगत की उत्पत्ति’ के विषय में बताया गया है। अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाते हुए ब्रह्मऋषि उद्दालक ने कहा कि सृष्टि के प्रारम्भ में एक मात्र ‘सत्’ ही विद्यमान था। फिर किसी समय उसने अपने आपकों अनेक रूपों में विभक्त करने का संकल्प किया।
उसके संकल्प करते ही उसमें से ‘तेज’ प्रकट हुआ। तेज में से ‘जल’ प्रकट हुआं संकल्प द्वारा प्रकट होने वाले उस ‘तेज’ को वेद में ‘हिरण्यगर्भ’ कहा गया है। सृष्टि का मूल क्रियाशील प्रवाह यह ‘जलतत्त्व’ ही है, जो तेज से प्रकट होता है। उस जल के प्रवाह से अतिसूक्ष्म कण बने और कालान्तर में यही सूक्ष्म कण एकत्र होकर ‘पृथ्वी’ का कारण बने। प्रारम्भ से सृष्टि-सृजन की पहली आहुति द्युलोक में ही हुई थी। उसी में विद्यमान ‘सत्’ से ‘तेज’ और तेज से ‘जल’ की उत्पत्ति हुई थी तथा जल के सूक्ष्म पदार्थ कणों के सम्मिलन से पृथिवी का निर्माण हुआ था। धरती से अन्न का उत्पादन हुआ तथा दूसरे चरण में सूर्य उत्पन्न हुआ।
दूसरा, तीसरा और चौथा खण्ड :
सृष्टि का त्रिगुणात्मक स्वरूप
इन दोनों खण्डों में सृष्टि के त्रिगुणात्मक स्वरूप की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि ने तीन प्रकार के जीव उत्पन्न कियें इन प्राणियों के ये तीन बीज-‘अण्डज, ‘ ‘जरायुज’ और ‘उद्भिज’ कहलाये। तब सत्य-रूपी तेज ने उपर्युक्त तीनों बीजों से तीन-तीन जीवात्मा रूप उत्पन्न किये। ये तीनों रूप ‘कारण, ‘सूक्ष्म’ और ‘स्थूल’ रूप में प्रकट हुए। इस त्रिविधि प्रवृत्ति के अनुरूप ‘तेज’ (अग्नि), ‘जल’ और ‘अन्न’ के भी तीन-तीन रूप हुए। उनके वर्ण इस प्रकार हैं
- अग्नि- का वर्ण ‘लाल’ (तेज, प्रकाश), (जलतत्त्व का रूप) ‘श्वेत’ वर्ण और (अन्नतत्त्व का रूप) ‘कृर्ष्ण’ वर्ण है।
- आदित्य (सूर्य)— की लालिमा प्रकाश-रूप है, श्वेत वर्ण जलतत्त्व है और कृर्ष्ण वर्ण अन्न-रूप हैं।
- इसी प्रकार ‘चन्द्र’ और ‘विद्युत’ के वर्ण भी बताये गये हैं।
पांचवां और छठा खण्ड :
तेज, जल, अन्न का त्रिगुणात्मक रूप
इन खण्डों में ‘तेज,’ ‘जल’ और ‘अन्न’ का त्रिगुणात्मक विवेचन किया गया है।तेज- जो तेज ग्रहण किया जाता है, वह तीन रूपों में विभाजित हो जाता है। उस तेज का स्थूल भाग ‘हड्डी’ के रूप में, मध्यम भाग ‘मज्जा’ के रूप में और अत्यन्त सूक्ष्म अंश ‘वाणी’ रूप में परिणत हो जाता है।जल- ग्रहण किये गये जल की परिणति भी तीन प्रकार से विभक्त होती है। जल का स्थूल भाग ‘मूत्र’, मध्यम अंश ‘रक्त’ और सूक्ष्म अंश ‘प्राण’ बन जाता है।अन्न- ग्रहण किया गया अन्न भी तीन भागों में बंट जाता है। अन्न का स्थूल भाग ‘मल,’ मध्यम अंश ‘मांस’ और जो अतिसूक्ष्म है, वह ‘मन’ के रूप में परिवर्तित हो जाता है।उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाया कि ‘तेज’ का कार्य ‘वाणी’ है, जल का कार्य ‘प्राण’ है और ‘अन्न’ का कार्य ‘मन’ है।
जिस प्रकार दही के मथने से उसका सूक्ष्म भाव मक्खन के रूप में एकत्र हो जाता है, वही प्रवृत्ति ऊर्ध्व की ओर गमन करने की है। इसी प्रकार तेज, जल और अन्न का सूक्ष्म भाग, मन्थन के उपरान्त क्रमश: ‘वाणी’, ‘प्राण’ और ‘मन’ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य यही है कि तेज से ‘वाणी, ‘जल से ‘प्राण’ और अन्न से ‘मन’ का निर्माण होता है।
सातवां खण्ड :
मन और अन्न का परस्परिक सम्बन्ध
इस खण्ड में ‘मन और अन्न का पारस्परिक सम्बन्ध’ बताया गया है। उद्दालक ने एक दृष्टान्त से इसे समझाया है। उन्होंने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा-‘हे वत्स! यह मनुष्य सोलह कलाओं को धारण कर सकता है। यदि तुम पन्द्रह दिन तक भोजन न करो और मात्र जल का ही सेवन करते रहो, तो तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं होगा; क्योंकि ‘प्राण’ को जल-रूप कहा गया है। केवल जल ग्रहण करने से जीवन का अन्त नहीं होता।’ु इस कथन की परीक्षा के लिए श्वेवकेतु ने पन्द्रह दिन तक भोजन नहीं किया।
वह जल द्वारा ही अपने प्राणों को पुष्ट करता रहा।पन्द्रह दिन बाद उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा कि अब वह जाये और वेदों का अध्ययन करे, किन्तु वह ऐसा नहीं कर सका। उसे मन्त्र याद नहीं होते थे। तब उद्दालक ने अपने पुत्र को भोजन करने के लिए कहा और फिर मन्त्र याद करने के लिए कहा।इस बार उसे मन्त्र याद हो गये। इससे पता चला कि जैसे जल ‘प्राण’ के लिए अनिवार्य है, उसी प्रकार अन्न भी ‘मन’ के लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार ‘वाणी’ तभी प्रस्फुटित होती है, जब ज्ञान का ‘तेज’ मनुष्य के भीतर होता है।
आठवां खण्ड :
जीवन-मृत्यु
इस खण्ड में ‘जीवन-मृत्यु’ के सन्दर्भ में अन्न, जल और तेज के महत्त्व को समझाते हुए उसके ‘सृजन’ ‘संहार’ क्रम का दर्शाया गया है कि कब इनका शरीर में तेजी से प्रादुर्भाव होता है और कब ये शरीर का साथ छोड़जाते हैं।
सोते समय पुरुष का शरीर सततत्त्व से जुड़ जाता हे। इसको ‘स्वयित,’ अर्थात ‘अपने आपको प्राप्त करने’ की स्थिति कहते हैं। जैसे डोरी से बंधा बाज पक्षी सभी दिशाओं में उढ़ने के उपरान्त पुन: अपने उसी स्थान पर आ जाता है, जहां वह बंधा है, वैसे ही यह मन इधर-उधर भटकने के उपरान्त शरीर का ही आश्रय ग्रहण करता है। शरीर में यह प्राणतत्त्व में विश्राम करता है। अत: यह मन प्राणों से बंधा है।
इस शरीर का मूल ‘जल’ और ‘अन्न’ ही है। शरीर जिस अन्न को ग्रहण करता है, उसे जल की शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। यह शरीर अन्नमय है। इसी प्रकार जल की गति का आधार तेज है, उर्ज्या है। इस प्रकार अन्न ग्रहण करते ही जल और तेज की क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसी से ‘जीवन’ का आधार तय होता है।
परन्तु ‘मृत्यु’ के समय शरीर सबसे पहले यह तेज, अर्थात अग्नितत्त्व छोड़ देता है। अग्नितत्त्व के जाते ही वाणी साथ छोड़ जाती है, परन्तु मन फिर भी सक्रिय बना रहता है; क्योंकि उसमें पृथ्वीतत्त्व प्रमुख होता है। अन्न के माध्यम से वह प्राण में निहित रहता है, किन्तु जब प्राण भी तेज में विलीन हो जाते हैं और तेज भी शरीर का साथ छोड़ देता है, तो शरीर मृत हो जाता है। धरती के अतिरिक्त अन्य सभी तत्त्व साथ छोड़ जाते हैं और शरीर मिट्टी के समान पड़ा रह जाता है। अत: इस शरीर में जो प्राणतत्त्व है, वही आत्मा है, परमात्मा का अंश है, वही सत है, वही जीवन है।
इस प्रक्रिया को सभी वर्तमान वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि शरीर के प्रत्येक कोश तक अन्न को, तेज की ऊर्ज्या से जल ही ले जाता है। इस प्रक्रिया के चलते ही शरीर जीवित रहता है और इस प्रक्रिया के रूकते ही शरीर मृत हो जाता है।
नौवें खण्ड से तेरहवें खण्ड तक :
ब्रह्म की सर्वव्यापकता
इन खण्डों में विविध पदार्थों के माध्यम से ‘ब्रह्म की सर्वव्यापकता’ को सिद्ध किया गया है। ब्रह्मऋषि उद्दालक अपने पुत्र से कहते हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खियां विभिन्न पुष्पों से मधु एकत्र करती हैं और जब वह मधु एकरूप हो जाता है, तब यह कहना कठिन है कि अमुक मधु किस पुष्प का है या उसे किस मधुमक्खी ने संचित किया है। इसी प्रकार जो ‘ब्रह्म’ को जान लेता है, वह स्वयं को ब्रह्म से अलग नहीं मानता।
श्वेतकेतु के पुन: पूछने पर उन्होंने दूसरा उदाहरण नदियों का दिया। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और अपना अस्तित्त्व समाप्त कर देती है, तब वे सागर के जल में विलीन होकर नहीं कह कसतीं कि वह जल किस नदी का है। उसी प्रकार उस परम ‘सत्व’ से प्रकट होने के उपरान्त, समस्त जीवात्माएं उसी ‘सत्व’ में विलीन होकर अपना व्यक्तिगत स्वरूप नष्ट कर देती हैं। सागर की भांति ‘ब्रह्म’ का भी यही स्वरूप है।
पुन: समझाने का आग्रह करने पर उन्होंने वृक्ष के दृष्टान्त से समझाया। वृक्ष की जड़ पर, मध्य में या फिर शीर्ष पर प्रहार करने से रस ही निकलता है। यह रस उस परम शक्ति के होने का प्रमाण है। यदि वह उसमें न होता, तो वह वृक्ष और उसकी डालियां सूख चुकी होतीं। इसी प्रकार यह वृक्ष-रूपी शरीर जीवनतत्त्व से रहित होने पर नष्ट हो जाता है, परन्तु जीवात्मा का नाश नहीं होता। ऐसे सूक्ष्म भाव से ही यह सम्पूर्ण जगत है। यह सत्य है और तुम्हारे भीतर विद्यमान ‘आत्मा’ भी सत्य और ‘सनातन ब्रह्म’ का ही अंश है।
इसके बाद ब्रह्मऋषि उद्दालक ने श्वेतकेतु से एक महान वटवृक्ष से एक फल तोड़कर लाने को कहा। फल लाने के बाद उसे तोड़कर देखने को कहा और पूछा कि इसमें क्या है? श्वेतकेतु ने कहा कि इसमें दाने या बीज हैं। फिर उन्होंने बीज को तोड़ने के लिए कहा। बीज के टूटने पर पूछा कि इसमें क्या है? इस पर श्वेतकेतु ने उत्तर दिया कि इसके अन्दर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तब ऋषि उद्दालक ने कहा-‘हे सौम्य! इस वटवृक्ष का यह जो अणुरूप है, उसके समान ही यह सूक्ष्म जगत है। वही सत्य है, वही सत्य तुम हो। उसी पर यह विशाल वृक्ष खड़ा हुआ है।’
श्वेतकेतु द्वारा और स्पष्ट करने का आग्रह करने पर ऋषि उद्दालक ने नमक के उदाहरण द्वारा उसे समझाया। उन्होंने नमक की एक डली मंगाकर पानी में वह नमक की डली पानी में निकालकर उसे दे दे, परन्तु वह उसे नहीं निकाल सका। फिर उन्होंने उसे ऊपर से, बीच से और नीचे से पीने के लिए कहा, तो उसने कहा कि यह सारा पानी नमकीन है। तब ऋषि उद्दालक ने श्वेतकेतु को समझाया कि जिस प्रकार वह नमक सारे पानी में घुला हुआ हैं और तुम उसे अलग से नहीं देख सकते, उसी प्रकार तुम उस परम सत्य ‘ब्रह्म’ के रूप को अनुभव तो कर सकते हो, पर उसे देख नहीं सकते। यह सम्पूर्ण जगत भी अतिसूक्ष्म रूप से ‘सत्यतत्त्व’ आत्मा में विद्यमान है। यही ‘ब्रह्म’ है। जब तक यह तुम्हारी देह में विद्यमान है, तभी तक तुम स्वयं भी ‘सत्य’ हो।
चौदह से सोलह खण्ड तक :
सूक्ष्म आत्मा क्या है?
श्वेतकेतु के पुन: पूछने पर ऋषि उद्दालक ने अगले तीन खण्डों में एक पुरुष की आंखों पर पट्टी बांधने, मरणतुल्य पुरुष की वाणी के चले जाने और अपराधी व्यक्ति द्वारा तप्त कुल्हाड़े को ग्रहण करने के उदाहरणों द्वारा सूक्ष्म तत्त्व आत्मा के सत्य स्वरूप को समझाया।आंखों पर पट्टी बांधकर ‘ब्रह्म’ अथवा ‘सत्य’ की खोज नहीं की जा सकती। व्यक्ति को ‘आत्मा’ और ‘परमात्मा’ के एक रूप को पहचानने में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान है।
मरणतुल्य प्राणी की वाणी तब तक मन में लीन नहीं होती, जब तक मन प्राण में जीन नहीं होता, प्राण तेज में जीन नहीं होता और तेज परमतत्त्व में लीन नहीं होता। तब तक वह अपने बन्धु-बान्धवों को पहचानता रहता है, परन्तु आत्मा के परमतत्त्व में विलीन होते ही वह किसी को नहीं पहचान सकता। जो अणु-रूप में विद्यमान है, वही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में चैतन्य-स्वरूप है। वही सत्य है, वही सभी प्राणियों में ‘प्राणतत्त्व’ है। वही ‘आत्मा’ है।
इसी प्रकार चोरी करने वाला अपराधी तप्त कुल्हाड़े को सत्य आवरण से नहीं ढक सकता और उसका स्पर्श करते ही उसके हाथ जल उठते हैं, किन्तु चोरी न करने वाला व्यक्ति अपने सत्य से तप्त कुल्हाड़े की गरमी को ढक लेता है। उस पर गरम कुल्हाड़े का किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ता।वस्तुत: यह समस्त विश्व ‘सत्य-स्वरूप’ है। वही ‘आत्मा है और वही परमात्मा’ है, वही परब्रह्म है, सत्य है, निर्विकार और अजन्मा है। वह अपनी इच्छा से अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है और स्वयं ही अपने भीतर समा जाता है।
सप्तम अध्याय
इस अध्याय में छब्बीस खण्ड हैं। इन शब्दों में ‘ब्रह्म’ से ‘प्राण’ तक की व्याख्या प्रस्तुत की गयी है। ‘ब्रह्म’ की वास्तविक स्थिति क्या है, उस पर प्रकाश डाला गया है।
एक से पन्द्रहवें खण्ड तक :
ब्रह्म का यथार्थ रस क्या है?
इन खण्डों में ऋषि सनत्कुमार नारद जी को ‘प्राण’ के सत्य स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। नारद जी चारों वेदों, इतिहास, पुराण, नृत्य, संगीत आदि विद्याओं के ज्ञाता थे। उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व था। एक बार उन्होंने सनत्कुमारजी से ‘ब्रह्म’ के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने नारदजी से यही कहा कि अब तक आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वह सब तो ब्रह्म का नाम-भर है।
उन्होंने कहा-‘नाम के ऊपर वाणी है; क्योंकि वाणी द्वारा ही नाम का उच्चारण होता है। इसे ब्रह्म का एक रूप माना जा सकता है। वाणी के ऊपर संकल्प है; क्योंकि संकल्प ही मन को प्रेरित करता है। संकल्प के ऊपर चित्त है; क्योंकि चित्त ही संकल्प करने की प्रेरणा देता है। चित्त से भी ऊपर ध्यान है; क्योंकि ध्यान लगाने पर ही चित्त संकल्प की प्रेरणा देता है। ध्यान से ऊपर विज्ञान है; क्योंकि विज्ञान का ज्ञान होने पर ही हम सत्य-असत्य का पता लगाकर लाभदायक वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। विज्ञान से श्रेष्ठ बल है और बल से भी श्रेष्ठ अन्न है; क्योंकि भूखे रहकर न बल होगा, न विज्ञान होगा, न ध्यान लगाया जा सकेगा। कहा भी है-‘भूखे भजन न होय गोपाला।’
उन्होंने आगे कहा-‘अन्न से भी श्रेष्ठ जल है। जल के बिना जीव का जीवित रहना असम्भव है। जल से भी श्रेष्ठ तेज है; क्योंकि तेज के बिना जीव में सक्रियता ही नहीं आती है। इसी क्रम में तेज से श्रेष्ठ आकाश है, आकाश से श्रेष्ठ स्मरण, स्मरण से श्रेष्ठ आशा और आशा से श्रेष्ठ प्राण है; क्योंकि यदि प्राण ही नहीं है, तो जीवन भी नहीं है। अत: यह प्राण ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है।’
सोलह से छब्बीस खण्ड तक :
सत्य से आत्मा तक ब्रह्म की यात्रा
इस खण्डों में ‘सत्य’ से ‘आत्मा’ तक व्याप्त ‘ब्रह्म’ के विविध स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। सनत्कुमार नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि ‘सत्य’ को जानने के लिए विज्ञान और विज्ञान को मानने के लिए बुद्धि-विशेष का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि के लिए श्रद्धा का होना अनिवार्य है। श्रद्धा द्वारा ही बुद्धि किसी विषय का मनन कर पाती है। श्रद्धा के साथ निष्ठा का होना भी अनिवार्य है; क्योंकि निष्ठा के बिना श्रद्धा का जन्म नहीं होता।
इसी प्रकार निष्ठा के लिए कृति का सामने होना आवश्यक है। ऐसी कृति सुख अथवा हर्ष प्रदान करने वाली होनी चाहिए। तभी कोई साधक उस पर निष्ठापूर्वक श्रद्धा रखकर व अपनी बुद्धि-विशेष से मनन करके, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर ‘सत्य’ की खोज कर पाता है।
‘भूमा’ क्या है?
भारतीय दर्शन में ‘भूमा’ शब्द का विशेष उल्लेख मिलता है। इस ‘भूमा’ शब्द का अर्थ है- विशाल, विस्तृत, विराट, अनन्त, असीम, विराट, अनन्त, असीम, विराट पुरुष, धरती, प्राणी और ऐश्वर्य । इस ‘भूमा’ की खोज ही भारतीय तत्त्व-दर्शन का आधार है। यह ‘भूमा’ अनन्त आनन्द की प्रदाता है। सांसारिक प्राणी इसी ‘भूमा’ का संसर्ग पाना चाहता है। यह ‘भूमा’ ही ‘ब्रह्म’ का स्वरूप है। इसे ही अमृत, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वोत्तम कहा गया है। यही ‘आत्मा’ है। इसे जान लेने के उपरान्त मनुष्य समस्त सांसारिक भोगों से मुक्त होकर शुद्ध रूप से अपने अन्त:करण में विद्यमान ‘परब्रह्म’ को प्राप्त कर लेता है।
अष्टम अध्याय
इस अध्याय में शरीर में स्थित ‘आत्मा’ की अजरता-अमरता का विवेचन किया गया है। इस अध्याय में पन्द्रह खण्ड हैं।
एक से छह खण्ड तक :
शरीर में ‘आत्मा’ की स्थिति
इन छह प्रारम्भिक खण्डों में शरीर के भौतिक स्वरूप में ‘आत्मा’ की स्थिति का वर्णन किया गया है और हृदय तथा आकाश की तुलना की गयी है। यहाँ आत्मा के इस प्रसंग को गुरु-शिष्य परम्परा के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। गुरु अपने शिष्यों से कहता है कि मानव-हृदय में अत्यन्त सूक्ष्म रूप से ‘ब्रह्म’ विद्यमान रहता है।
‘स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरूक्त्ँ हृद्ययमिति तस्माद्धदथमहरहर्वा एवंवित्स्वर्ग लोकमेति॥3/3॥’ अर्थात वह आत्मा हृदय में ही स्थित है। ‘हृदय’ का अर्थ है ‘हृदि अयम्’- वह हृदय में है। यही आत्मा की व्युत्पत्ति है। इस प्रकार जो व्यक्ति आत्मतत्त्व को हृदय में जानता है, वह प्रतिदिन स्वर्गलोक में ही गमन करता है।
वास्तव में जितना बड़ा यह आकाश है, उतना ही बड़ा और विस्तृत यह चिदाकाश हृदय भी है। इस हृदय में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में ‘आत्मा’ निवास करता है। यह शरीर समय के साथ-साथ जर्जर होता चला है और एक दिन वृद्ध होकर मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इसीलिए शरीर को नश्वर कहा गया है, परन्तु इस शरीर में जो ‘आत्मा’ विद्यमान है, वह कभी नहीं मरता। वह न तो जर्जर होता है, न वृद्ध होता है और न मरता है।
मनुष्य अज्ञानतावश हृदय में रहने वाले इस ‘ब्रह्मरूपी आत्मा’ को नहीं जान पाता। इसलिए वह मोह-माया के सांसारिक बन्धनों में बंधा रहता है, परन्तु ज्ञानी व्यक्ति ‘आत्मा’ को ही ‘ब्रह्म’ का रूप जानकर ओंकार (प्रणव) तक पहुंच जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ‘ब्रह्मज्ञानी’ कहलाता है। जो साधक ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते हुए हृदयलोक में स्थित ‘ब्रह्म’ के सूक्ष्म रूप ‘आत्मा’ को जान लेते हैं, उन्हें ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सम्पूर्ण लोकों में वे अपनी इच्छाशक्ति से कहीं भी जा सकते हैं।
सातवें से पन्द्रहवें खण्ड तक :
‘आत्मा’ का यथार्थ रूप
इन खण्डों में इन्द्र और विरोचन को उपदेश देते हुए प्रजापति ब्रह्मा ‘आत्मा’ के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं।एक बार देवराज इन्द्र और असुरराज विरोजन प्रजापति ब्रह्मा के पास ‘आत्मा’ व ‘ब्रह्मज्ञान’ के यथार्थ सत्य को जानने की जिज्ञासा से पहुंचते हैं और उनके पास रहकर बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं; क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना ‘ब्रह्म’ की प्राप्त नहीं की जा सकती।
बत्तीस वर्ष पूर्ण होने पर प्रजापति ब्रह्मा ने उनके आने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने ‘ब्रह्मरूप और ‘आत्मा’ के स्वरूप को जानने के लिए अपनी जिज्ञासा प्रकट की। इस पर ब्रह्मा ने कहा कि हम जो कुछ भी आंखों से देखते हैं, वह ‘आत्मा’ का ही रूप है। यह सुनकर दोनों ने दर्पण मं अपने स्वरूप को देखकर अपने प्रतिबिम्ब को ही ‘आत्मा’ मान लिया तथा दोनों अपने-अपने लोकों को लौट गये।विरोचन ने असुरों के पास जाकर कहा कि यह अलंकृत शरीर ही ‘आत्मा’ है। इसे ही ‘ब्रह्म’ का स्वरूप समझो और इसी की उपासना करो।
उधर इन्द्र ने देवलोक पहुंचने से पहले सोचा कि यह नश्वर शरीर नष्ट हो जायेगा, तो क्या ‘आत्मा’ अथवा ‘ब्रह्म’ भी नष्ट हो जायेगा। उसे सन्तुष्टि नहीं हुई, तो वह पुन: ब्रह्मा के पास लौटकर आया और अपनी शंका प्रकट की। ब्रह्मा ने उसे पुन: बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा। बत्तीस वर्ष बाद ब्रह्मा ने इन्द्र से कहा कि पुरुष के जिस रूप का मनुष्य स्वप्न में दर्शन करता है, वही ‘आत्मा’ है। इन्द्र ऐसा सुनकर चला गया, किन्तु मार्ग में उसे फिर शंका ने आ घेरा कि स्वप्न में देखे गये पुरुष की आकृति जागने पर नष्ट हो जाती है, यह ‘ब्रह्म’ नहीं हो सकता। वह पुन: ब्रह्मा के पास लौट आया और अपनी शंका प्रकट की। तब ब्रह्मा ने उसे पुन: बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा। इन्द्र ने ऐसा ही किया और पुन: ब्रह्मा के पास जा पहंचा।
तब ब्रह्मा ने कहा कि जो प्रसुप्त अवस्था में सम्पूर्ण रूप से आनन्दित और शान्त रहता है और स्वप्न का अनुभव भी नहीं करता, वही ‘आत्मा’ है। वही अनश्वर, अभय और ‘ब्रह्म’ है। इन्द्र सन्तुष्ट होकर चल दिया। उसने सोचा कि उस समय जीव को यह कैसे ज्ञान होगा कि वह कौन है और कहां से आया है? अत: यथार्थ ज्ञान शरीर से सम्बन्धित हुए बिना कैसे प्राप्त हो सकता है? शंका उत्पन्न होते ही वह पुन: ब्रह्मा के पास जा पहुंचा और अपने मन की शंका प्रकट की। इस पर ब्रह्मा ने उसे पांच वर्ष तक पुन: ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए कहा। इस प्रकार इन्द्र ने कुल एक सौ एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया।
तब ब्रह्मा ने उससे कहा-‘हे इन्द्र! यह शरीर मरणधर्मी है एवं सदैव मृत्यु से आच्छादित है। अविनाशी तथा अशरीरी ‘आत्मा’ इस शरीर में निवास करता है। जब तक यह शरीर में रहता है, तब तक प्रिय-अप्रिय से घिरा रहता है। शरीर से युक्त होने के कारण वह उनसे मुक्त नहीं हो पाता, किन्तु जब यह शरीर छोड़कर अशरीरी हो जाता है, तब प्रिय-अप्रिय कोई भी इसे स्पर्श नहीं कर पाता। तब वह ‘आत्मा’ आकाश में वायु की भांति ऊपर उठकर इस शरीर को छोड़ते हुए परमज्योति में केन्द्रित हो जाता है। इस प्रकार जो यथार्थ ‘आत्मा’ है, वह सूर्य की ज्योति से प्रकट होकर शरीर में प्रवेश करता है, किन्तु मृत्यु के समय शरीर के सभी सुख-दु:ख से मुक्त होकर यह पुन: उसी ‘आदित्य’ में समा जाता है। यही ‘ब्रह्म है।’ इन्द्र इस बार पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होकर इन्द्रलोक को चला गया।