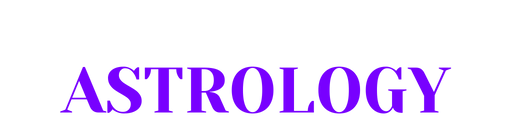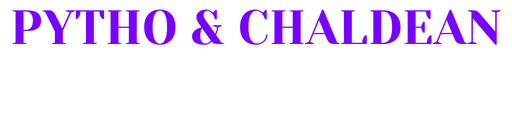देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र – Devi Apradh Kshamapan Stotra
कलियुग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत प्रसिद्ध और प्रामाणिक हैं। प्रामाणिक इस कारण से हैं क्यूंकि इस युग में भी वो द्वापर, त्रेता और यहाँ तक कि सतयुग के भाव का आभास कराती हैं। माता के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में जितना लिखा गया है उतना कदाचित किसी और पर नहीं लिखा गया है। कहा जाता है कि माता के वश में तो स्वयं नारायण रहते हैं।
किन्तु उन सब में भी जो एक चीज कलियुग में सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो ये एक वाक्य है – “पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।” किन्तु क्या आप जानते हैं कि इसे सर्वप्रथम किसने, क्यों और किसके लिए कहा था? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये वास्तव में शाश्वत सत्य है जैसा कि आज के युग में माना जाता है? आइये इस विषय में कुछ जानते हैं।
वास्तव में ये उद्धरण “देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र” के एक श्लोक का एक वाक्य मात्र है। इस श्लोक की रचना अदि शंकराचार्य ने की थी। ये स्त्रोत्र पूर्ण रूप से माता दुर्गा को समर्पित है जिसमें आदि शंकराचार्य माता से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं। इस स्तोत्र में कुल १२ श्लोक हैं और इनमें से तीन श्लोकों के अंतिम वाक्य में आदि शंकराचार्य ने माता के महत्त्व के विषय में कहा है।
आइये देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र का अर्थ भी समझ लेते हैं।
न मत्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः ।
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् ॥१॥
अर्थात: हे माँ! मैं न मंत्र जनता हूँ न यंत्र, अहो! मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। न आह्वान का पता है न ध्यान का। स्तोत्र और कथाओ कभी ज्ञान नहीं है। न तो मैं तुम्हारी मुद्राएँ जनता हूँ और ना ही मुझे व्याकुल होकर विलाप ही करना आता है। परन्तु एक बात जनता हूँ कि तुमारा अनुसरण करना तथा तुम्हारी शरण में आना सब क्लेशों एवं सब विपत्तियों को हरने वाला है।
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत् ।
तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥२॥
अर्थात: हे माँ! सबका उद्धार करनेवाली कल्याणमयी माता! मैं पूजा की विधि नहीं जनता। मेरे पास धन का भी अभाव है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक-ठीक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटी हो गई है उसे क्षमा कर देना क्योंकि पुत्र का कुपुत्र होना तो संभव है किन्तु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः
परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः ।
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥
अर्थात: माँ! इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे सादे पुत्र तो बहुत से हैं किन्तु उन सब में ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसे चंचल कोई बिडला ही होगा। शिवे! मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किन्तु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता
न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया ।
तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥४॥
अर्थात: जगदम्बा! माता! मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी! तुम्हे अधिक धन भी समर्पित नहीं किया। तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो इसका कारण यह है कि संसार में कुपुत्र तो पैदा हो सकता है पर कहीं भी कुमाता नहीं हो सकती।
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया
मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि ।
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता
निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम् ॥५॥
अर्थात: हे श्री गणेश को जन्म देनेवाली माता! मुझे नानाप्रकार की सेवाओं में मुझे व्यग्र रहना पड़ता था इस लिए ८५ वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब होकर किसकी शरण में जाऊंगा?
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः ।
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥६॥
अर्थात: हे माता अपर्णा! तुम्हारे मन्त्र का एक भी अक्षर मेरे कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होगा कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के सामान मधुर वाणी उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य करोड़ो मुद्राओं से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भर विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधिपूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त उत्तम फल कैसा होगा? इसको कौन मनुष्य जान सकता है?
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो
जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः ।
कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् ॥७॥
अर्थात: भवानी! जो अपने अंगो में चिता की राख लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा एवं कंठ में नागराज वासुकि को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी, जो एक मात्र “जगदीश” की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणिग्रहण की परिपाटी का फल है। अर्थात तुम्हारे साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया है।
न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः ।
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै
मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥८॥
अर्थात: मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ! मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की अकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव-शिव भवानी, इन नामों का जपते हुए बीते।
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः
किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः ।
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥९॥
अर्थात: माँ श्यामा! नानाप्रकार के पूजन सामग्रियों से सभी विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी । सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरे वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है? फिर भी तू स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि जो रखती हो, माँ! यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारे जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है।
आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं
करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि ।
नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥१०॥
अर्थात: माता दुर्गे! करुणासिंधु महेश्वरी! मैं विपत्तियों में फंस कर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ (और इससे पहले कभी नहीं किया) इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख-प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते है।
जगदम्ब विचित्रमत्र किं
परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि ।
अपराधपरम्परापरं
न हि माता समुपेक्षते सुतम् ॥११॥
अर्थात: हे जगदम्बे! मुझ पर तुम्हारी कृपा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की बात है। पुत्र अपराध पर अपराध करता जाता हो फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती।
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि ।
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु ॥१२॥
अर्थात: हे महादेवी! मेरे सामान कोई पातकी (पाप करने वाला) नहीं और तुम्हारे सामान कोई पाप हरिणी नहीं। ऐसा जानकर जो उचित पड़े वो करो। ये श्लोक निःसंदेह माता के महत्त्व को प्रदर्शित करता है किन्तु ये भी समझना आवश्यक है कि आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना विशुद्ध रूप से माँ दुर्गा के लिए की थी और इसमें जो माता का उद्बोधन है वो भी माँ भवानी के विषय में ही है। किन्तु शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक चीज का भाव देश और काल के अनुरूप बदलता है। इसी कारण इस कलिकाल में इसे प्रत्येक स्त्री के लिए शाश्वत सत्य भी नहीं माना जा सकता। कदाचित इसी कारण आदि शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना कलियुग में की ताकि आने वाले समय में ये समाज का मार्ग प्रशस्त कर सके।